शिव प्रकाश त्रिपाठी का नयी दिल्ली के पुस्तक मेले पर रिपोर्ताज ‘बहुरि न आवहु हट्ट...’।
नयी दिल्ली में हर वर्ष जनवरी का
महीना पुस्तक-प्रेमियों के लिए ‘पुस्तक-मेले’ की सौगात ले आकर आता है। प्रकाशक इस अवसर
पर अपनी विशिष्ट किताबों की श्रृंखला प्रकाशित और प्रस्तुत करते हैं। कई लेखक
पुस्तक मेले की उत्सुकता से प्रतीक्षा इसलिए करते हैं क्यों कि मेले में उनकी
किताब के आने और विमोचित होने का कार्यक्रम पहले से ही सुनिश्चित होता है। कई लेखक
साल भर मेहनत की कमाई से प्रति महीने बचाए हुए अपने कोष से कुछ चुनिन्दा किताबें
खरीदने के लिए आते हैं। और हमारे जैसे तमाम मित्र, अगर पारिवारिक व्यस्तताओं से
समय निकाल पाए तो, (क्योंकि हम सबके लिए दिल्ली अक्सर दूर ही होती है) अपनी खाली
ज़ेबें लिए घूमने-टहलने और मित्रों-परिचितों से मिलने के लिए मेले में पहुँच जाते
हैं। युवा कवि शिव त्रिपाठी ने इस पुस्तक मेले पर एक उम्दा रिपोर्ताज़ लिख भेजा है।
(रिपोर्ताज हिन्दी साहित्य की उन विधाओं में से एक है, जो पहले काफी लिखे जाते थे।
लेकिन समय की मार रिपोर्ताज पर भी पड़ी है और अब तो कविता-कहानी-उपन्यास के मकड़जाल
ने जैसे सारी विधाओं और रिपोर्ताज को जैसे लील सा लिया है।) शिव ने बड़ी रोचक शैली
में यह रिपोर्ताज लिखा है जिसमें गँवई मेले और बोली-बानी की सुगन्ध मिल जाएगी। लेकिन
शिव की नज़र आज के जमाने की दिखावटी लेखकीय-अभिजात्यता की बू भी पडी है और उन्होंने
इसकी भी ख़बर ली है। आज पहली बार पर प्रस्तुत है शिव प्रकाश त्रिपाठी का नयी दिल्ली के पुस्तक मेले पर रोचक
रिपोर्ताज ‘बहुरि न आवहु हट्ट...’।
बहुरि न आवहु हट्ट... ... ...
शिव प्रकाश त्रिपाठी
मेले-ठेले का नाम सुनते ही कहीं भीतर बैठा बचपन गुलाटी मारने लगता
है, जैसे कि चुटकी काटने पर चिहुंक के उठता है कोई। मेला जीवन को परिष्कारित करता
है। न सिर्फ हमारे विचारों को एक बड़ा फलक देता है अपितु तमाम रुग्णताओं, कुंठाओं
और अजनबीपन आदि को दूर कर समाज को प्रक्षालित करता है व उसे सौहार्दपूर्ण बनाता है।
जहाँ एक तरफ आम-जनों का संगम कराता है वहीं विभिन्न विशेषताओं से युक्त समाजों और
संस्कृतियों के मिलन में भागीदार भी बनाता है। मेला तो फिर मेला ही हुआ। किसिम
किसिम की दुकानें, दुकानों में जुटी भीड़ और भीड़ का फायदा उठाते हुए कुछ जोशीले
नौजवान। मेले में आदमी और कुछ खाए न खाए धक्के जरुर खाता है। बरबस कैलास गौतम का
‘अमौसा का मेला’ याद आ जाता है। कमाल की बात देखिए दिल्ली में पुस्तक मेला लगा हुआ
है और हम भी सशरीर मौजूद हैं। तो इस विचार के साथ कि आज सिर्फ और सिर्फ मेला
घूमेंगे, जाने का समय निर्धारित किया गया। दरअसल यही मूल अंतर है मेला और बाजार में
है भी, क्योंकि बाज़ार खरीददार की मांग करता है मेला घुमक्कड़ों की और मेला का असली
मज़ा तो तभी है जब तक कि दू-चार फेरा पूरा लगाया न जाय। मेले में तरह तरह की आवाज़ों
के मेल से रचता एक अद्भुत संगीत और ऐसे ही माहौल के बीच छुपते-छुपाते बड़े ही संकोच
के साथ मिलती हैं दो जोड़ी आँखें, जिनमें इंतज़ार की लम्बी रेखाएं स्पष्टतः देखी जा
सकती हैं। मेले में घटित अनेक घटनाएँ जो बनती है कालांतर में किवदंतियाँ। तरह-तरह
के गप्प, महीनों बाद गाँव में ठंड में कौड़ा तापते होती है इन पर चर्चा। बुजुर्गों
का नए लड़कों के ग़दर काटने पर उन्हें कोसना और ननकउना जैसे दू चार चिल्लरों का इन
गप्प से अपने मतलब की बातों को ढूढना... ... यह प्रक्रिया चलती रहती है महीनों।
तो बड़े उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करते हुए, मेले के पूर्व नियोजित
कार्यक्रम को अमली-जामा पहनाया गया फलस्वरूप हम भी पहुँच गये प्रगति मैदान। मेले
में प्रवेश के लिए शुल्क निर्धारित किया गया था। टिकट काउंटर मेट्रो स्टेशन में ही
बनाया गया था। इंट्री फ़ीस सुन कर अटपटा लगा क्योंकि हमारे गाँव के मेले में तो कभी
कोई फ़ीस नहीं लगती बल्कि कई दफ़े हमारी मण्डली ने उलटे मेला में आई दुकानों से
उगाही की, कभी क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पर तो कभी किसी नाम पर। पर यहाँ तो उलटे
हमें पैसे देना पड़ रहा था पर धीरे-धीरे समझ आया कि ‘ये तो दिल्ली है मेरी जान’। पर
तभी अपनी कमाई काम आई मतलब अपनी दोस्ती-यारी...। इन्हीं ने हमें मेला में प्रवेश
दिलाया। इस बेरोजगार के पास कमाई के नाम पर कुछ बेहतरीन दोस्त और कुछ स्नेही व बड़े
भाई सदृश वरिष्ठ-जन ही हैं। तो धीरे-धीरे जा पहुँचा हाल नम्बर 12-A के ठीक सामने। ये
हाल मेंन गेट से दो बाधा द्वार पार करते हुए दाहिने हाथ मुड़ते ही चेहरे के ठीक
सामने पड़ता है। मशीन के नीचे से गुजरते
हुए खुद को प्रवेश कराया इन किताबों की दुनिया में। यहाँ भी ये मेला मेरे गाँव के मेले
से अलग दिख रहा है, दरअसल ये मेले जैसा नहीं, मॉल जैसा दिख रहा है। जिस कम्पनी की
जितनी हैसियत उतनी ही आकर्षक सजावट से तनी हुई दुकानें। बस एक ही बात देख मन को
सुकून मिला की भीड़ चौचक है , मने खूब धक्कम-धक्का और जी भर ठेलमठेल मची हुई है।
फिर क्या था हमने भी भीड़ में घुसा दिए खुद को। ये भीड़ देख उत्साह की गिरावट का क्रम
टूटा और अब बचे हुए उत्साह से मेला घूमने का विचार कौंधा। हमने फ़ौरन खुद को इस
विचार के हवाले कर दिया। फिर क्या था मस्ती से जैकेट के जेब में दोनों हाथ डाल
घुमने लगा दुकान दर दुकान और काउंटर दर काउंटर। घूमने के दौरान बहुत से आभासी
दुनिया यांनी फेसबुक से बने मित्र भी मिले। जिनमें कुछ तो पूरे जोश-ओ-ख़रोश के साथ मिले पर ज्यादातर किसी
चमकदार चीज के इन्तजार में दिखे। उन्हें हम जैसे अनगढ़ चीजों से कोई लगाव न दिखा। हम
से बात करते हुए भी उनकी एक जोड़ी आँखे ढूढ़ रही थीं चमकदार चीजे जिसके साहचर्य से
उन्हें भी कुछ प्रतिदीप्ति मिलती। वो झट ऐसे लोगो के पास जा कर सबूत इकठ्ठा कर रहे
थे यानी कि सेल्फी ले रहे थे जिसे वो गर्व से दुनिया को दिखा सकें। दरअसल एक समय
बाज़ार का ये बड़ा हथकण्डा रहा है खुद को लाइमलाइट में लाने का। बाज़ार बड़े लोगो को
खुद से जोड़ कर अपने को प्रमोट करने में लगा रहा और आज-कल कुछ नव-साहित्यकारों ने
इसे अपना रखा है। चूँकि समयाभाव था तो इन सब विषय पर ज्यादा न सोचते हुए फिर जुट
गये मेला घूमने में बिना खरीददारी किये हुए क्योंकि हम लगभग कसम जैसी चीज खा कर
आये थे कि सिर्फ और सिर्फ मेला घूमेंगे, खरीददारी एक्को नहीं करेंगे
लेकिन ये मेला फिर हमरे गाँव जैसा नहीं निकला।
हम अपने गाँव के मेले में घूमते ज्यादा थे खरीदते कम। अब भला इस मॉल नुमा मेले में
इतना घूमना कहाँ संभव था। तो हम भी बाज़ार के माया-जाल में फंस गये। जितनी भी
करेंसी थी सब लुटा दिए। बाजार तो जादूगर निकला। हम कब कंगाल हुए ये तब पता चला जब
जेब खाली और बैग भरा पाया। अब इसमें पूरा दोष बाजार का भी नहीं है। कुछ किताबों के
प्रति मोह का भी है। मोह कब आपके विचारों को पूरी तरह ढाप ले पता ही नहीं चलता। हा
मोह में भले ही आप डूबेंगे नहीं पर किसी किश्ती की तरह मोह के आवेग में दूर तक बह
सकते हैं। खैर जब होश में आये तो पूरी तरह से खाली हो चुके थे। अब थकावट महसूस हो
रही रही है, बाहर खुले आसमान के नीचे सुस्ताने का विचार आया और फिर हम विचार के
साथ हो लिए पर इस बार सतर्कता के साथ। हाल से बाहर निकला तो वहाँ भी निराशा हाथ
लगी। जहाँ एक बड़ी सी पेट-पूजा की दुकान हुआ करती थी वहाँ दैत्याकार मशीनें अपना
मुँह बाए खडी थी। उसने लील लिया था वो दुकान और उससे सटी हुई हरी घास का वह कोना
भी जहाँ पिछले दफ़ा हम बैठ सुस्ताये थे...।
मेला में मुख्यतः तीन प्रकार के जीव ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ
बछड़े हैं जो बचे हुए मैदाननुमा जगह में कुलांचे भर रहे हैं, कुछ खूंटे है जो शायद
दुधारू गाय के तलाश में निकले हैं और तीसरे किसिम के ‘दुधारू जीव’ अपने उत्पाद के
प्रमोशन के सिलसिले में अपने प्रमोटर के दरवाजे पर रँभा रहे हैं। बछड़े निसफिकिर हो
मैदान में रच रहे हैं अपना एक अलग संसार। इनकी सामूहिक एकता पर बरबस ध्यान खिंच
जाता है। ये अपने दुलत्तियों को उठा संतुलन साधने का जोखिम उठा रहे हैं। दरअसल ये
प्रशिक्षण वह अपने अनुभवी वरिष्ठों से ही सीख रहे हैं। ऐसे कामों में जोखिम बहुत
होता है पर वह युवा ही क्या जो जोखिम से डर जाए। इनमें कुछ युवा बड़े आनन्द के साथ इन जोखिम से
भरे कुछ रचनात्मक प्रगतिशील कामों में भी जुटे हुए हैं। इन सब के बीच थोड़ा सुकून समेटते
हुए फिर एक बार जा पहुँचा उस विशालकाय हाल में जो हमारे गाँव के न बचे हुए ‘रहूनी’
से भी बड़ा है। यहाँ मै देख रहा हूँ कुछ खूंटों का दुधारू जीवों से अद्भुत मिलन।
खूंटों की आँखों में जो चमक दिख रही है ठीक वैसी ही चमक उन दुधारुओं में नहीं है
एवं जो हालत इन जीवों की है उसको देख खूंटे को किसी उर्वर भूमि में गड़ने का बल मिल
रहा है। इस हाल में मुझे कुछ विरोधाभासी स्थितियां दिखाई दे रही हैं जहाँ एक तरफ
बछड़े एकजुट हो साथ-साथ पूरे मेले का आनन्द ले रहे हैं वहीं उनके वरिष्ठ स्वयं के
साथ यत्र-तत्र विचरण कर रहे हैं, जिनके चेहरे में बनावटी मुस्कान स्थायी भाव बन
चुकी है। वह सिर्फ पूंछ हिलाने वाले का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ख़ुद को
विशिष्ट बनाने के चक्कर में शायद भूल गये थे कि लोग उन पर हँस रहे हैं। कुछ लोग
तरस जैसे सहानुभुतिपरक भावों से उन्हें अभिसिंचित कर रहे थे।
ये सब देखना वाकई दुखद है कि जो कैमरे की चमक में इतने सहिष्णु और
लोकतान्त्रिक दिखाई देते हैं असलियत में उसके ठीक उलट हैं। हम बछड़ों को क्या मिल
रहा है इस पीढ़ी से सिर्फ छलावा, छद्मता, कुंठा जैसी अनेक थातियाँ, जो रच रहीं है
निराशा, हताशा और अवसरवादिता जैसे भावों और शब्दों का एक संसार। एक पीढ़ी के द्वारा
दूसरे पीढ़ी को आखिर दिया क्या जा रहा है? इतनी संवादहीनता शायद पहले नहीं रही होगी
दो पीढियों के बीच कभी? इन दुधारू जीवों को वही रास आ रहे हैं जो इनके खाने में
पिसान और घर का बचा हुआ चोकर चला रहे हैं, जिसे ये खा रहे हैं चभर-चभर। बछड़े दूध
को तरस रहे हैं। दूध अब उत्पाद बन चुका है जिसे कर दिया गया है बाजार के हवाले।
बाजार ऐसे ही उत्पादों को तो बेचने के लिए ही रचता है, मेले जैसा आभास देता बाज़ार,
जिसके मूल में एक ही भावना होती है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना।
थकावट, हताशा और उदासी से भरा हुआ भारी मन लेके अपने पिट्ठू बैग के साथ
लौट रहा हूँ, अपने थाने-पवाने। बिलकुल बुझे हुए लालटेन सा। ये मेला यहाँ भी मेरे
गाँव जैसा मेला नहीं दिखा क्योंकि हर बार अपने गाँव के मेले से लौटने पर मै भरा
होता था एक उर्जा से। शरीर हवा से हल्का लगता था हर बार। हर बार असीम और अनंत जैसे
शब्द मेरे भीतर कुलाँचे भरते रहते थे, पर यहाँ तो मै धरती से भी भारी महसूस कर रहा
हूँ खुद को। मेला तो जोड़ता है हमें और हमारे समाज को बनाता है ज्यादा सहिष्णु,
ज्यादा लोकतान्त्रिक और ज्यादा प्रगतिशील। मेला सांस्कृतिक जागरण में सहयोग देता
है, वह कभी हताशा नहीं देता! उसके यहाँ निराशा व हताशा जैसे शब्दों के लिए कोई जगह
नहीं होती। ये मेला मेरे गाँव वाला मेला बिलकुल नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि
यह तो मेला ही नहीं है मेले का नकाब लगाये मॉल की आत्मा वाला एक जादूगर है, यह बाजार
है । ऐसे जादूगरों से बचना मेरे साथियों, इनकी भाषा चाशनी में डुबोई भी हो सकती है। मै अबकी लौट रहा था मेले से असीम और अनंत जैसे शब्दों
के बिना ही... ...।
सम्पर्क -
फोन - 08960580855
ई-मेल : ssptripathi2011@gmail.com
(इस पोस्ट की तस्वीरें गूगल के सौजन्य से ली गयी हैं.)
(इस पोस्ट की तस्वीरें गूगल के सौजन्य से ली गयी हैं.)





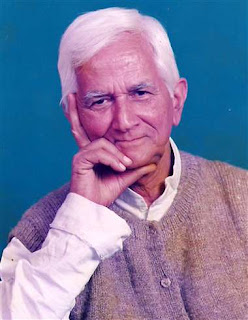


बहुत बढ़िया
जवाब देंहटाएं